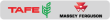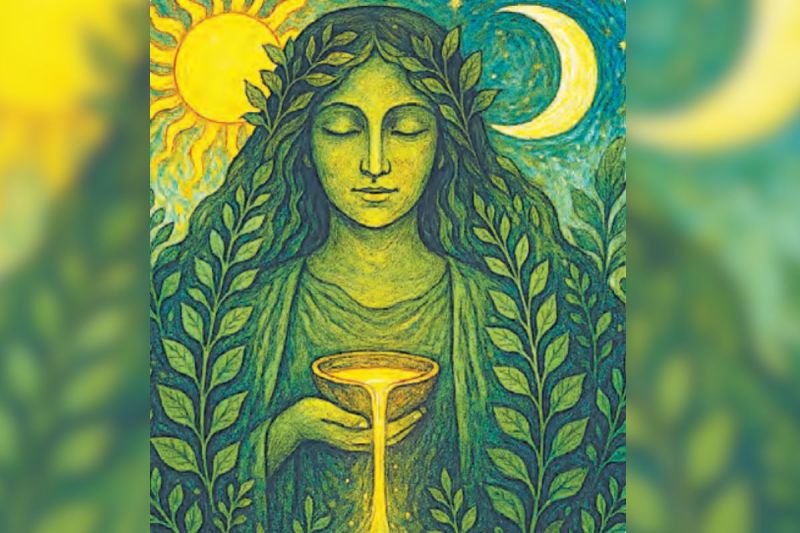
फोटो: पत्रिका
'एकोऽहं बहुस्याम्’—यह कामना ही मन का पहला बीज है—वेद का उद्घोष है—कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेत: प्रथमं यदासीत्। यही गॉड पार्टिकल है। निराकार भी है और क्रिया शून्य भी है। स्थूल साधनों से कैसे पकड़ सकते हैं। स्थूल से आगे सूक्ष्म सृष्टि है। सूक्ष्म के आगे सुसूक्ष्म जगत है। उसके परे ब्रह्म है। कामना पदार्थ भी नहीं है। इसमें क्रिया भी नहीं है। सभी 84 लाख योनियों की सृष्टि में एक ही ब्रह्म, एक ही कामना है, निरन्तर प्रवाहित है। इसी कामना की पूर्ति हेतु निर्विशेष ब्रह्म क्रमश: परात्पर, पुर व पुरुष रूप में सृष्टिक्रम में आगे बढ़ते हैं। पुरुष ही अव्यय है जो ऋक्, यजु: व साम रूप वेदत्रयी हैं। ऋक्-साम को महदुक्थ एवं महाव्रत कहते हैं। यजु ही पुरुष है। सूर्य का प्रकाश मण्डल महदुक्थ है, रश्मिमण्डल महाव्रत है। केन्द्र में गति रूप प्राणाग्नि पुरुष है, गति के गर्भ में स्थिति भी है। यही मौलिक तत्त्व है। ऋक्-साम इसी की प्रतिष्ठा है।
यह पुरुष कामभाव से क्षुब्ध होता है जिसके कारण प्राण भाग अप् (आप) रूप में बदल जाता है। अव्यय का जो भाग क्षुब्ध हो जाता है, वह आप बन जाता है, शेष भाग ज्यों का त्यों स्व-स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है। एक ही प्रजापति प्राण-आप भेद से दो भागों में विभक्त हो जाता है। प्राण वृषा भाग पुरुष है, आप योषा भाग स्त्री है।
तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत् सिद्धान्त के अनुसार स्वयंभू, परमेष्ठी रूप आप की सर्जना करके उसमें प्रवेश कर जाते हैं। स्वयंभू के पारमेष्ठ्य महान् (भृगु-अंगिरामय) में प्रवेश करने से ही अण्डवृत्त का स्वरूप बनता है। तभी ब्रह्माण्ड स्वरूप अश्वत्थ का विकास होता है। स्वयंभू आपोमय महान् के गर्भ में प्रविष्ट होकर ही कामबीज को अंकुरित कर पाते हैं। अत: इस मनोमय कामबीज का मूल बीजत्व भी आपोमय महान् पर ही अवलम्बित है। बीज पानी में ही अंकुरित होता है। अव्यय मन को चूंकि अश्वत्थ वृक्ष में बढ़ना है, अत: अपने कामबीज को अप् तत्त्व से ही समन्वित करना पड़ता है। महान् ही अव्यय को अपने गर्भ में निहित करके इसे विश्व वृक्ष रूप दे देता है।
सत्यम्, तप:, जन:, मह:, स्व:, भुव: तथा भू सप्त लोकों में से मह:लोक सूर्य से ऊपर है। पृथ्वी और चन्द्रमा सहित सूर्य इनकी परिक्रमा करते हैं। पार्थिव संस्कार से महान् में आकृति भाव का उदय होता है। चन्द्रमा से प्रकृति तथा सूर्य से अहंकृतिरूप अहं भाव का उदय होता है। बोलचाल के अहंकार का कोई सम्बन्ध नहीं है इससे। भूपिण्ड रूपज्योति है, तमो भावात्मक है। चन्द्रमा परज्योति, रजो भावात्मक है। सूर्य स्वज्योति भाव से सत्त्व भावात्मक है। इस प्रकार परमेष्ठी महान् षड्भावात्मक बन जाता है। विश्व पंचपर्वा होते हुए भी अमृत-मृत्यु भेद से षट् रूप माना गया है। स्वयंभू-परमेष्ठी-सूर्य अमृत विश्व है, तथा सूर्य-चन्द्रमा-भूपिण्ड मर्त्य विश्व है। ऊपर रसप्रधान है, नीचे बलप्रधान है—तद्यत् किंचार्वाचीनमादित्यात्-सर्वं तन्मृत्युनाऽप्तम्। सूर्य मध्यस्थित है। तीनों अमृत प्राणों—ऋषि, पितर तथा देव का संबंध तीनों मर्त्य प्राणों से क्रमिक रूप में होता है। सूर्य ऋषि प्राण का प्रवर्तक है, चन्द्रमा देव प्राण का तथा भूपिण्ड पितर प्राण का संग्राहक है। अत: तीनों प्राणों का क्रमश: महान् के अहंकृति-प्रकृति-आकृति से समन्वय हो जाता है।
तमोगुण युक्त, पार्थिव पितर भाव युक्त, पारमेष्ठ्य महान के आकृति भाग से प्राणियों के शरीर का निर्माण हेाता है। रजोगुण युक्त चन्द्रमा के देवभाग से समन्वित प्रकृति भाव से प्रकृति का स्वरूप बनता है। सत्व गुण से युक्त और ऋषि भाग से समन्वित महान के अहंकृति भाव से बुद्धि का स्वरूप निर्माण होता है। अव्ययात्मा केवल मानव में होता है। केन्द्रस्थ आत्म तत्त्व का नाम मनु है। इसके विकास से ही प्राणी मानव कहलाता है। मानव के शरीर में प्रतिष्ठित पार्थिव पितर प्राण से मानव 'जाति’ का विकास हुआ। आकृति की समानता से सभी मानव समान हैं। चान्द्र मन में प्रतिष्ठित देव प्राणों से मानव के 'वर्ण’ का विकास हुआ है। मानव जाति एक ही है, किन्तु वर्णयुक्त (प्रकृतिमूलक वर्ण-अवर्ण भेद से) आठ भागों में विभक्त है—चातुर्वण्र्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागश:।
बुद्धि में प्रतिष्ठित सौर ऋषि प्राण 'गोत्र’ भाव का विकास हुआ है। गोत्र विभिन्न वंशों के अनुसार भिन्न-भिन्न हैं। अव्यक्तात्मा जाति, वर्ण, गोत्र तीनों भावों का प्रवर्तक है। स्वयं अगोत्र, अवर्ण, समान है। जाति से वर्ण, वर्ण से गोत्र श्रेष्ठ है।
अव्यक्तात्मा ही अव्यय है। इसकी दो प्रकृतियां परा और अपरा ही अक्षर व क्षर कहलाते हैं। अव्यय-अक्षर-क्षर ही क्रमश: कारण-सूक्ष्म-स्थूल शरीर कहलाते हैं। इनमें अव्यय पुरुष है और अक्षर-क्षर प्रकृति है। सबका आलम्बन पुरुष भाव है। वेदत्रयी रूप इसी का यजु: भाग मूल पुरुष है, ऋक्-साम प्रतिष्ठा है। सूक्ष्म भाग हृदय रूप है—ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र अक्षर प्राणों का समूह है। बाह्य पृष्ठ में अग्नि-सोम दो प्राण रहते हैं। अव्यय के पांच प्राण या कलाएं जहां अमृत रूप हैं, वही हृदय की कलाएं ब्रह्म कहलाती हैं। इन्हीं से क्षर पुरुष की पांच कलाएं—प्राण, आप्, वाक्, अन्नाद, अन्न उत्पन्न होती हैं। इनका अमृत रूप शुक्र कहलाता है तथा मर्त्य रूप क्षर ब्रह्म।
अक्षर पुरुष का अमृत/मर्त्य में विभाजन होता है और क्षर पुरुष का भी। अमृत भाग परा प्रकृति तथा मर्त्य भाग अपरा प्रकृति रूप में कार्य करते हैं। अमृत सृष्टि सूक्ष्म तथा मर्त्य सृष्टि स्थूल बनती है। पुरुष-स्त्री दोनों में कारण शरीर अमृत है तथा सूक्ष्म तथा स्थूल रूप मर्त्य-प्रकृति है। अमृत भाव निष्कल रहता है, मर्त्य भाव पंचकल रूप है। प्रकृति को ज्ञान-क्रिया-अर्थ रूप कहा है जो कि वैश्वानर, तैजस, प्राज्ञ रूप जीवात्मा ही है। अमृत आत्मा ईश्वर आत्मा है—विराट्, हिरण्यगर्भ, सर्वज्ञ रूप है। ईश्वर प्राण शरीर के हृदय में प्रतिष्ठित रहता है। जीवात्मा भी भोक्ता रूप में (द्वासुपर्णा) साथ रहता हैं। ज्ञान भाग का आधार पुरुष में प्रधान रहता है तथा क्रिया और अर्थ भाग प्रकृति (स्त्री) में प्रधान होता है। ब्रह्म निष्क्रिय रहता है- कामना मात्र करता है। कारण शरीर कामना का केन्द्र रूप मन है। इसके अमृत भाग में प्रकृतिदत्त (पूर्व कर्म फल रूप) कामना पैदा होकर कर्मरूप स्थूल देह में क्रिया रूप में प्रकट होती है।
कर्म कामनाओं पर आधारित रहते हैं, अत: प्रत्येक कर्म का फल भी निश्चित है। अमृत कामना के कर्म तो स्वयं फलरूप ही होते हैं। हमारी चेष्टा से बाहर होते हैं। जीवात्मा के नए कर्म नए फलों को जन्म देते हैं। ये संचित कर्म के रूप में पुन: कारण शरीर में जुड़ जाते हैं। इनके फल और भोग काल भी परा प्रकृति ही तय करती है। किन्तु सारे कर्म, चाहे अमृत सृष्टि के हो, अथवा अपरा प्रकृति के- शरीर में इनका नियंत्रण एवं संचालन स्त्रैण रूप में होता है। जीवात्मा की कामना मर्त्य मन में उठती है। इन्द्रियों के विषयों द्वारा और स्थूल देह में रूपान्तरित होती है। स्थूल देह कामनाओं का ही प्रतिबिम्ब है। दोनों की स्थूल देह माता द्वारा निर्मित मर्त्य भाव ही है। जीवात्मा का संस्कार-पोषण भी परा रूप में माता ही करती है। मूल में सम्पूर्ण सृष्टि कर्म माता के ही हाथ में है। गर्भ में माता द्वारा तथा बाद में प्रकृत रूप में।
चूंकि पुरुष का स्त्रैण भाग अधिकांशत: अपूर्ण ही रहता है, अत: उनकी क्रियाएं भी अमृत रूप न होकर सभी मर्त्य रूप में नए कर्मफलों को उत्पन्न करती हैं। इसी प्रकार शिक्षित स्त्री का पौरुष भाव प्रधानता लिए रहता है, स्त्रैण भाव गौण होता जाता है। सौम्यता का स्थान उष्णता ले लेती है। यहां भी प्रकृति से विरुद्ध नए कर्मों का निर्माण होता है। गर्भावस्था के कर्म भी गौण हो जाते हैं। इस कारण भी (इसके अभाव में) नए फल संचित में जुड़ते जाते हैं।
अमृत और मर्त्य सृष्टि के मध्य का तारतम्य टूट रहा है। प्रकृति का नया ताण्डव विश्व में दिखाई देने लगा है। धीरे-धीरे सौम्यता विदा हो रही है, संवेदना विदा हो रही है। क्रिया भाव तटस्थ है। ज्ञान के अभाव में अविद्या ही नए कर्मों का संचालन-नियंत्रण करने लगी है। दैविक सम्पदा का स्थान शनै:शनै: आसुरी सम्पदा लेती जा रही है। जैसी कामना, जैसा बीज, वैसे ही फल!
क्रमश: gulabkothari@epatrika.com
Published on:
23 Aug 2025 09:28 am
बड़ी खबरें
View Allओपिनियन
ट्रेंडिंग