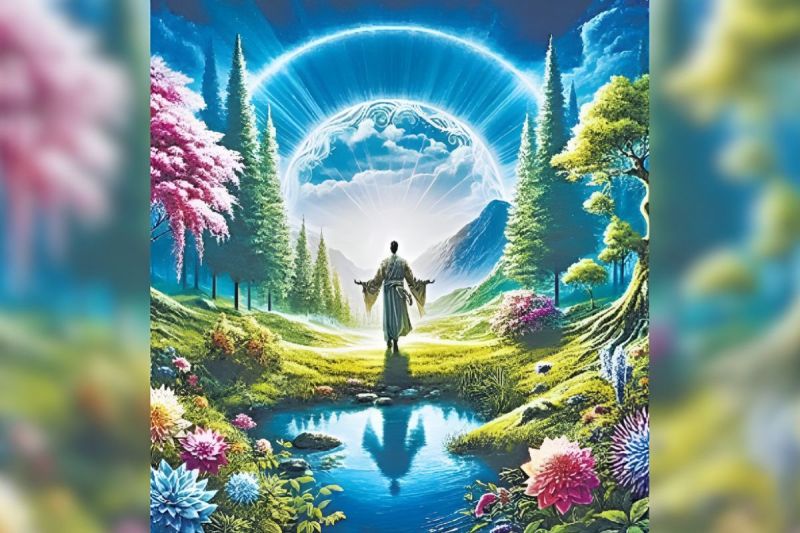
फोटो: पत्रिका
आत्मा पहले एक था, पुरुषविध था। ‘मैं हूं’ पहले यह वाक्य कहा- बृह.आ. 1.4.1, 1.4.3 तब दूसरे की कामना की—‘स द्वितीयमैच्छत्’ फिर अनेक हुआ- ‘सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेय इति’। ‘मैं लोकों की सृष्टि करूं’। सृष्टि में सब पुरुष हैं, ईश्वर ही पुरुष है, सृष्टि पुरुष प्रधान है। आत्मा पुरुष है- शाश्वत है। शरीर नश्वर है, प्रकृति है। प्रकृति का चक्र पुरुष के आधार पर चलता है, प्रकृति संचालक है। पुरुष सूक्ष्म स्तर पर प्रतिष्ठित है, प्रकृति उसकी कर्मरूप अभिव्यक्ति है।
पुरुष आत्मा रूप में और शरीर- महिमा रूप में रहता है। पुरुष का रस प्रकृति में सिक्त होकर प्रकृति की वस्तु बन जाता है। प्रकृति पृथ्वी का पर्याय है। पुरुष प्रजापति स्वरूप है। शरीर विच्छेद के साथ इनका सबन्ध विच्छेद नहीं होता। प्रकृति शरीर से पुरुष-रस समय-समय पर (पृथ्वी पर तीन वर्ष) दक्ष और वरुण प्राण के साथ बाहर निकलता रहता है। चारों ओर के वायुमण्डल में उपस्थित वायु (एमूष वराह) ही दिक् सोम से मिलकर ‘दक्ष’ बनता है। परमेष्ठी समुद्र का अंभ: जो पृथ्वी से संयुक्त होता है-‘वरुण’ कहलाता है। दक्ष और वरुण दोनों पृथ्वी की वाक् में रिसते रहते हैं।
पृथ्वी के आग्नेय वाक् और दक्ष (सौय) तथा वरुण (आप्य) प्राणों के संघर्ष से वैश्वानर (वसु) अग्नि उत्पन्न होता है। इसी वसु अग्नि में तीनों के योग से भृगु-अंगिरा-अत्रि तीन प्राण उत्पन्न होते हैं। अग्नि में जो लौ का भाग है उससे भृगु प्राण पैदा होता है। ऊपर से जो आप्य प्राण इस अग्नि में शामिल होता है, वह दक्ष के साथ ही होता है। दक्ष की सौयता से ही आग्नेय प्राण प्रज्ज्वलित होता है। अत: आप्य ही सौयप्राण का उपलक्षण है। ज्वाला के नीचे लाल अग्नि पिण्ड से अंगिरा प्राण पैदा हुआ। वरुण को दक्ष का उपलक्षण कहा है। पृथ्वी से बाहर जाता हुआ संवत्सर अग्नि ही अंगिरा का जनक है। तथा पृथ्वी से जितना निराकार (ऋत रूप) वाक् का हिस्सा निकलता है- वह अत्रि प्राण है। पृथ्वी आत्रेयी कहलाती है।
पुरुष-प्रकृति का यह सबन्ध शाश्वत है। साथ ही ‘यथाण्डे तथा पिण्डे’ के अनुसार सपूर्ण ब्रह्माण्ड में समान रूप से कार्य करता है। स्त्री सोम है, अत: भोग की स्वाभाविक प्रवृत्ति-अग्नि में आहुत होनी- रहती है। सभी मादा प्राणियों में यही प्रवृत्ति रहती है। विवेक मानव में रहता है। सृष्टि में दो धाराएं हैं—‘द्वे धारे स्वतंत्र रूपत्वात्’ (धर्मपाद 55) मीमांसा का मत है कि स्त्री धारा पुरुष धारामयी होकर ही कैवल्य प्राप्त करती है—‘स्त्री धारा पुंधारामयी कैवल्याधिकारिणी’। ( धर्मपाद 56)
अग्नि सत्य है, साकार है। सोम निराकार है, ऋत है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अकेले दोनों ही अर्थहीन हैं। अग्नि को अस्तित्व के लिए सोम चाहिए। सोम बन्द, अग्नि मंद। सोम को निराकार होने से सत्य का आश्रय चाहिए। अग्नि में सोम की आहुति ही यज्ञ है। निर्माण की प्रयोगशाला है। सोम ही निर्माण सामग्री का स्रोत भी है। सोम सृष्टि का बीज है। अग्नि में प्रवेश करके पेड़ बनता है, सृष्टि पैदा करता है। यही सोम की दिव्यता है।
अग्नि के भीतर सोम रहता है, सोम के भीतर अग्नि है। यही अर्द्धनारीश्वर का सिद्धान्त है। पुरुष भीतर स्त्री है, सोम है, अत: शुक्र से सौय है। स्त्री भीतर पुरुष है, आग्नेय है, शोणित अग्नि है। पुरुष के स्त्री भाग का विकास नहीं होता। भारतीय परिवारों में स्त्री पूर्ण विकसित होती है। विवाह के साथ उसका माया भाव भी जाग्रत होता है। दोनों मिलकर परात्पर बन जाते हैं। ब्रह्म के मन में कामना का उदय होता है- ‘एकोऽहं बहुस्याम्।’
जीवन सभ्यता और संस्कृति का समन्वय ही है। सभ्यता समय के साथ बदलती जाती है। संस्कृति का आधार आत्मा के संस्कार हैं। इनका मूल स्वरूप गर्भ में ही बन जाता है। कर्मों के फल विभिन्न योनियों में जन्म लेने के कारण है। स्त्री-पुरुष शरीर मां के गर्भ में एक ही अन्न से बने हैं। संस्कार भेद (गर्भ में) तथा प्रारब्ध भेद से व्यक्तित्व भिन्न हो जाते हैं। अन्न से मन बनता है, कामनाएं बदलती जाती हैं। स्त्री भीतर जीती है, पुरुष बाहर जीता है। स्त्री मन के आधार पर- सौया प्रकृति- कार्य करती है, परोक्ष भाषा में विश्वास रखती है, अत: दिव्यता का भाव भी रखती है—‘परोक्ष प्रिया इव हि देवा।’ शान्त रहकर स्थान में जीती है। पुरुष उष्ण है, बुद्धि प्रधान है, समय में जीने वाला है। स्त्री सोम, पुरुष अग्निप्रधान है। आपस में स्पर्धा करने के लिए अपने स्वरूप में परिवर्तन करना पडे़गा।
जीवन की सारी यात्रा सूक्ष्म जीवात्मा की है—परा प्रकृति की है। अपरा प्रकृति तो नया शरीर धारण करने के बाद ही स्वरूप ग्रहण करती है। कन्या का आत्मा पुरुष-जीवात्मा को ढूंढ़ लेता होगा। उसी को स्वयं की ओर आकृष्ट करता होगा। दोनों के माता-पिता की प्रकृतियां भी तो आपस में सबद्ध हाेंगी। वे भी प्रकृति की इस योजना में भागीदार होंगे ही। इन सबके पूर्व जन्मों के परस्पर ऋणात्मक सबन्ध भी होंगे जिनको अगले जन्मों में भोगना भी है। इतना ही नहीं, दोनों के अपने-अपने स्वजन/परिजन भी ऋणानुबन्ध के अनुसार साथ चलते होंगे।
भारतीय विवाह में शरीर केवल साधन बनते हैं। विवाह दो आत्माओं का होता है। ये सूक्ष्म स्तर की क्रियाएं हैं। पहले सौया की देह पुरुष की अग्नि में आहुत होती है। सौया का हर अंश स्वाहा हो जाता है। पति के आत्मा में लीन हो गई। लौटने को कुछ नहीं बचा। सृष्टि का बीज पुरुष के पास होता है, कन्या के हिस्से का अंश पिता के पास ही रहता है। विवाह के दौरान यह अंश दामाद के अंश में समाहित कर दिया जाता है। अब स्त्री का जीवात्मा पूर्ण रूप से पति के आत्मा से युक्त हो गया। पति की सात पीढ़ियों के अंश पत्नी तक पहुंच कर इस सबन्ध को सात जन्म का बना देते हैं।
स्त्री का शरीर एक उपकरण मात्र रह जाता है। वह तो पति के साथ सूक्ष्म- प्राण स्तर- भाव में जीने लग जाती है। प्राणों का स्तर दिव्य लोक है। यहां उसे चेतना रहती है कि वह ब्रह्म के विस्तार के लिए यहां आई है। भोग उसका लक्ष्य नहीं रहता। पहले वह पति के अधूरे स्त्रैण भाग को पूर्ण करने का प्रयास करती है। उसके पौरुष की उष्णता, आक्रामकता को शीतल करती है। उसे पूर्णता देती है। अब वह पुरुष की ‘शक्ति रूपेण संस्थिता’ वाली भूमिका में होती है।
नया मेहमान उसके जीवन का उद्देश्य होता है। वह ब्रह्मांश ही है। वह गर्भ में इस देव को धारण करके अत्यन्त गौरवान्वित होती है। ब्रह्म के विवर्त की उसकी भूमिका पूर्ण होने जा रही है। यह बोध पुरुष को नहीं होता। मां का भाव तंत्र इतना गहरा होता है कि दूरी या बाधा या काल कोई उसे रोक नहीं सकता। उसकी शक्ति उस काल में माया के तुल्य होती है। ब्रह्म का रक्षण-पोषण और अंधकार के दैत्य, सभी स्तरों पर दक्षता लिए होती है। मानो विष्णु की नाभि कमल पर ब्रह्मा का आवरण बनी हो।
-क्रमश: gulabkothari@epatrika.com
Published on:
29 Nov 2025 08:38 am
बड़ी खबरें
View Allओपिनियन
ट्रेंडिंग
