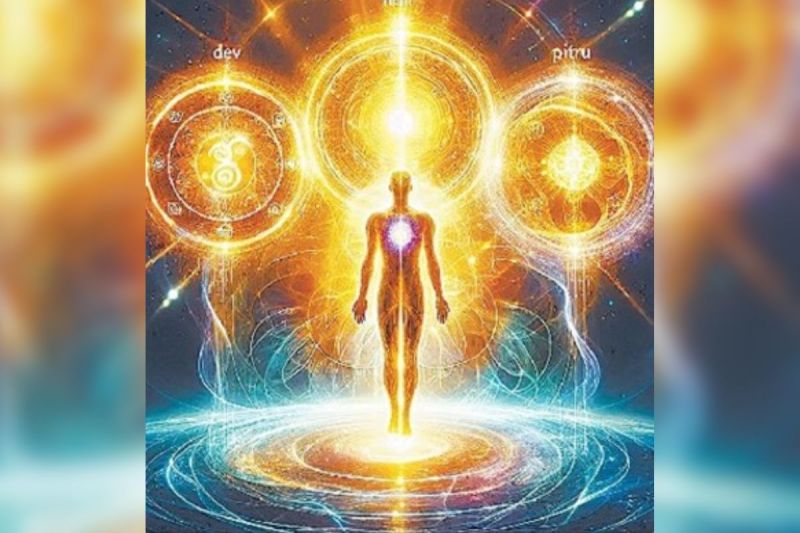
फोटो: पत्रिका
जीव तीन ऋण लेकर पैदा होता है जो कि सृष्टि के ही प्राण रूप होते हैं। जीवन तो प्राणों का ही पर्याय है। प्राणों से ही चलता है। प्राण निकल जाने पर ठहर जाता है। सातों लोकों का अपना प्राणों का स्वरूप है। सृष्टि में एकमात्र प्राण ही गतिमान तत्त्व है। सृष्टि में प्रत्येक कर्म शुरू होता है कामना से। प्राण ही कामना को गति देता है।
सूर्य जगत का पिता है। यहीं से षोड़शकल सृष्टि शुरू होती है। सूर्य देवलोक है। यहां के प्राण देव कहलाते हैं। सूर्य के आगे पितृलोक की स्थिति है। इस परमेष्ठी लोक के प्राण पितर प्राण कहलाते हैं। सबसे आगे स्वयंभू लोक- ऋषि प्राणों का लोक है। ये तीनों ही प्राण सभी प्राणियों का आत्मा बनते हैं। सभी प्राणी आत्मरूप ही हैं। कर्मों के अनुसार शरीर भिन्न-भिन्न होते हैं। सौम्य पितृ प्राण और आग्नेय ऋषि प्राण ही परमेष्ठी लोक में भृगु-अंगिरा रूप लेते हैं। यही अग्नि-सोमात्मक जगत के मूल प्राण हैं, जो आगे चलकर देव प्राणों की उत्पत्ति करते हैं। सृष्टि की दो धाराएं भृगु (लक्ष्मी) और अंगिरा (सरस्वती) रूप में आगे बढ़ती हैं। लक्ष्मी अर्थवाक् के रूप में तथा सरस्वती शब्दवाक् के रूप में आगे बढ़ती रहती है।
स्वयंभू अव्यय पुरुष रूप सृष्टि का प्रथम सत्य रूप है, ब्रह्मा है। यही प्राणियों का कारण शरीर बनता है, आलम्बन बनता है। इसी के कारण सृष्टि को पुरुष प्रधान कहा जाता है। इसी के मन को श्वोवसीयस मन कहते हैं। मन भी मूल में सभी प्राणियों का एक यही है। अन्य मन इसी के प्रतिबिंब रूप मन होते हैं। इसी मन की एक दिशा सृष्टि की ओर बढ़ती है। इसी की विपरीत दिशा मुक्ति की ओर जाती है।
ऋषि-पितर-देव प्राण ही जीवन के निर्माता प्राण हैं। इन्हीं का ऋण चुकाने की बात हमारे शास्त्र करते हैं। इस तथ्य को ध्यान में बनाए रखने के लिए हमें—'मातृ देवो भव’, 'पितृ देवो भव’ तथा 'आचार्य देवो भव’ सिखाया जाता है। ये क्रमश: क्षर-अक्षर-अव्यय सृष्टि के कारक हैं। अक्षर-क्षर ही क्रमश: परा-अपरा प्रकृतियां हैं—
भूमिरापोऽनलो वायु: खं मनो बुद्धिरेव च।
अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा।। (गीता 7.4)
पंचमहाभूत-मन-बुद्धि-अहंकार ही शरीर रूपी अपरा प्रकृति है। शरीर पार्थिव पंचमहाभूतात्मक है, मन चान्द्र है, बुद्धि सौरी है जो सूर्य के अहंकृति से उत्पन्न होती है। पृथ्वी से अन्न, अन्न से देह का निर्माण होता है। पृथ्वी भी लक्ष्मी है, देह भी लक्ष्मी है। शरीर को ही अन्नमय कोश (स्थूल) कहते हैं।
प्राणियों का शरीर गर्भ में तैयार होता है। माता के शरीर से, जो स्वयं अन्न से निर्मित है। अन्न से ही मन का निर्माण होता है। शरीर ही जीवात्मा का बाहरी आवरण (पृथ्वी रूपा) है। पृथ्वी भी जल से उत्पन्न होती है और शरीर भी जल से। शरीर की आकृति भी पृथ्वी और प्रकृति चन्द्रमा से बनती है। केन्द्र को ही मन कहते हैं। प्राणों द्वारा अन्न की चिति ही शरीर है। शरीर ही मां है। मातृ देवो भव। सन्तान की देह का निर्माण माता की देह से ही होता है। अन्न ही शरीर है, अन्न ही मन है, अन्न ही जीवात्मा है, अन्न ही ब्रह्म है। सृष्टि की प्रत्येक रचना में ये तीनों धरातल होते हैं। मानव में विशेष रूप से स्वतंत्र कर्म करने एवं पुन: अंशी तक लौट जाने की क्षमता है। चूंकि उसका मन चंचल है, उसे नियंत्रण-संचालन की आवश्यकता रहती है। इसी कारण पुरुष के साथ परा-अपरा प्रकृति बनाई, तीनों ही स्तरों पर यह कार्य करती हैं।
मां देह रूप अपरा है, अन्नमय कोश है। जननी है, पोषक है। अन्न ही मन है। मां मन भी है। भावनाओं का गंभीर-गहन धरातल है। संवेदना, प्रेम, वात्सल्य, सुख-दु:ख आदि तो मन के ही गुण हैं। चूंकि सन्तान भी अद्र्धनारीश्वर होती है, अत: मन के स्त्रैण भाव-पौरुष भाव भी मां ही प्रेषित करती है। इसके बिना सन्तान में स्त्रैण भावों का अभाव रह जाता है। इसके अभाव में पुरुष के स्त्रैण भाग सदा अपूर्ण ही दिखाई देंगे। ऐसे पुरुष सदा अहंकारी एवं आक्रामक ही दिखाई पड़ते हैं। उनमें आसुरी सम्पदा प्रमुख होती है। मां का अपरा रूप ही प्रेम और एकात्म भाव का क्षेत्र है। यह हृदय का क्षेत्र है जहां जीवात्मा के साथ मां की भूमिका दिखाई पड़ती है। मां के मन के स्पन्दन सन्तान के मन को प्रभावित करते हैं। संस्कारित करते हैं।
मां का दिव्य रूप सृष्टि कर्ता के रूप में देखा जाता है। मां यहां माया है। माया के कार्यों को केवल ब्रह्म ही समझ सकता है। यहां भाषा का तो पूर्ण अभाव ही रहता है। इशारों-संकेतों अथवा भावनाओं का सम्प्रेषण होता है। पुरुष को आमंत्रण, ईश्वर से प्रार्थना (शुद्ध आत्मा के लिए) तथा पुरुष के शरीर में व्याप्त ब्रह्मांश को एकत्र करके अपने शरीर में आहुत करना (इसका तो पुरुष तक को भान नहीं होता) कोई साधारण क्रिया नहीं है। ब्रह्म ने इसी आत्म विवर्त की चाहना की थी- एकोऽहं बहुस्याम्।
जीवात्मा के स्वरूप का ज्ञान, उसके पूर्व संस्कारों का परिष्कार करके भावी जीवन के अनुरूप संस्कार देना भी स्थूल क्रिया नहीं हो सकती। मां परा भाव में यह कार्य करती है। बिना किसी उपकरण के। उस जीव को यथानुरूप यथोचित ज्ञान देती है। जो न दिखाई देता है, न देख सकता है, न सुन सकता है, न ही बोल पाता है। पिता वै जायते पुत्र: अर्थात् पिता ही पुत्र बनता है। पिता भी देह रूप है। भीतर मातृ देह में बन्द रहता है। बीज रूप होता है, शरीर में प्रवाहित रहता है। इसी के साथ पिता की छह पीढ़ियों के अंश भी रहते हैं। पिता सन्तान में बीज रूप तैयार होता है (पुत्र में)। इस कर्म में सोलह (16) वर्ष लगते हैं। तब पुत्र नई सन्तान उत्पन्न करने में सक्षम होता है।
पिता के शुक्र में ही वर्ण भी समाहित रहता है। यह बीज पुत्री तक नहीं पहुंच पाता। अत: विवाह काल में मंत्रों द्वारा दामाद की आत्मा में प्रतिष्ठित करता है। तब आगे की संतानें पूर्ण होती हैं। गुरु भी दैहिक रूप में जुड़ता है। दीक्षा के माध्यम से शिष्य के साथ एकात्म भाव पैदा करके उसे पुत्र रूप में तैयार करता है। स्थूल के साथ सूक्ष्म का ज्ञान कराता है। सृष्टि के सभी रहस्यों, ध्यान साधना, तपादि के द्वारा हृद् प्राणों को विकसित करता है।
जीवन संकल्प-विकल्प के बीच झूलता रहता है। विकल्पों के बाहर निकलकर ही इच्छाशक्ति अथवा संकल्प-शक्ति शिष्य का निर्माण करती है। शिष्य का समर्पण भाव ही गुरु-शक्ति से कृपा प्राप्त करने में सफल होता है, तभी व्यक्ति की प्राण शक्तियां केन्द्रीभूत हो पाती हैं तथा पाप के क्षय का मार्ग प्रशस्त हो पाता है। गुरु का ज्ञान और शिष्य का कर्म मिलकर पूर्णता तक पहुंचकर ही प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। यही गुरु की महिमा है। बिना गुरु के जीवन में पूर्णता आना सम्भव नहीं। गुरु ही परम गुरु, परमेष्ठी-परात्पर गुरु रूप होकर जीवात्मा को अव्यय में लीन करा देता है।
क्रमश: gulabkothari@epatrika.com
Updated on:
08 Nov 2025 08:13 am
Published on:
08 Nov 2025 08:11 am
बड़ी खबरें
View Allओपिनियन
ट्रेंडिंग
